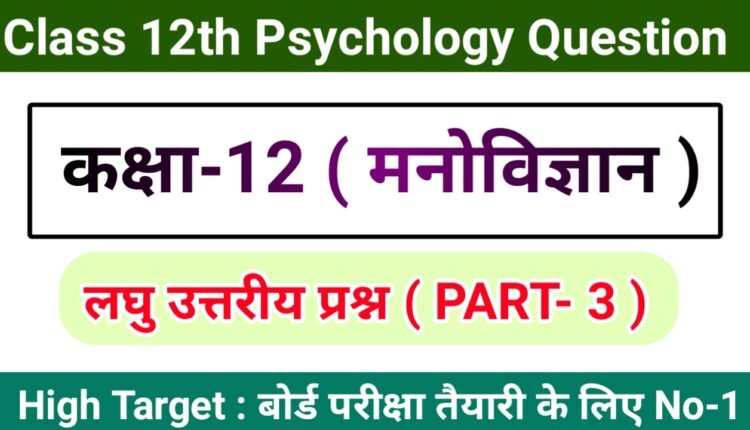Q.51. पूर्वाग्रह एवं रूढी धारण में अन्तर करें।
Ans ⇒ पूर्वाग्रह किसी विशेष समूह के प्रति अभिवृत्ति का उदाहरण है। अधिकांशतः यह A नकारात्मक होते हैं एवं विभिन्न स्थितियों में विशिष्ट समूह के सम्बन्ध में रूढ़धारणा पर आधारित होते हैं। रूढ़धारणा किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबद्ध विचारों का एक पुंज होती है। इस समूह के सभी सदस्य इन विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं। यह विशिष्ट समूह के सदस्यों के बारे में एक नकारात्मक अभिवृत्ति में पूर्वाग्रह को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर पूर्वाग्रह भेद-भाव के रूप में व्यवहार परक घटक में रूपान्तरित हो सकता है, जब लोक एक विशेष लक्ष्य समूह के लिए उस समूह की तुलना में जिसे वे पसंद करते हैं कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। प्रजाति एवं सामाजिक वर्ग या जाति पर आधारित भेदभाव की अनगिनत उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि कैसे पूर्वाग्रह घृणा, भेदभाव निर्दोष लोगों को सामूहिक संहार की ओर से आता है।
Q.52. संस्कृति और बुद्धि के संबंधों को लिखें।
Ans ⇒ बौद्धिक योग्यता पर सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि देहाती बच्चों की अपेक्षा शहरी बच्चे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। क्लाइनबर्ग (1966) के अनुसार शहर का वातावरण देहाती वातावरण की अपेक्षा अधिक उत्तेजक होता है, जिसके कारण बुद्धि के विकास में तेजी आती है। इस संबंध में प्रजाति-भिन्नता का भी अध्ययन किया गया, परन्तु कोई सामान्य निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सका। कैसरजहाँ (1982) ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अध्ययन में यह पाया कि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति वाले छात्रों की अपेक्षा उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति के छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च था। तामस (1983) तथा मिलग्राम (1988) ने भी समान निष्कर्ष प्राप्त किए।
Q.53. तनाव के किन्हीं दो प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें।
Ans ⇒ उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार अत्यधिक विस्तृत है जो दबाव को पैदा करती है। इनमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन में घटित होने वाली ये प्रमुख दबावपूर्ण घटनाएँ हैं, जैसे- किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु या व्यक्तिगत चोट, खीझ पैदा करने वाली दैनिक जीवन की परेशानियाँ, जो बेहद आवृत्ति के साथ घटित होती हैं तथा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली कुछ अभिघातज घटनाएँ।
1. जीवन घटनाएँ (Life incidents) – जब शिशु पैदा होता है, तभी से बड़े और छोटे, एकाएक पैदा होने वाले और धीरे-धीरे घटने वाले परिवर्तन शिशु के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। प्रायः इस छोटे तथा रोज होने वाले परिवर्तनों का सामना करना तो सीख लेते हैं लेकिन जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ दबावपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि वे हमारी दिनचर्या को अवरुद्ध करती है और हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा देती है। चाहे योजनाबद्ध घटनाएँ ही क्यों न हों (जैसे-घर बदलकर नए घर में जाना), जो पूर्वानुमानित न हो (जैसे-किसी दीर्घकालिक सम्बन्ध का टूट जाना) कम समयावधि में घटी हों, तो हमें उनका सामना करने में अत्यधिक परेशानी होती है।
2. परेशान करने वाली घटनाएँ (Difficult incidents) – ऐसे दबावों की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जो अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती है। रोज का आना-जाना, कोलाहलपूर्ण परिवेश, बिजली-पानी की कमी, यातायात की भीड़-भाड़, झगड़ालू पड़ोसी आदि कष्ट देने वाली घटनाएँ हैं। एक गृहणी को भी विभिन्न ऐसी आकस्मिक कष्टप्रद घटनाओं का अनुभव करना पड़ता है। कुछ व्यवसायों में कुछ ऐसी परेशान करने वाली घटनाओं का सामना निरंतर करना पड़ता है। कभी-कभी कुछ ऐसी ही परेशानियों का अधिक तबाहीपूर्ण परिणाम उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो घटनाओं का सामना अकेले करता है क्योंकि बाहरी अन्य व्यक्तियों को इन परेशानियों की जानकारी भी नहीं होती। जो व्यक्ति इन परेशानियों के कारण जितना ही अधिक दबाव महसूस करता है उतना ही अधिक उसका मनोवैज्ञानिक कुशल-क्षेम निम्न स्तर का होता है।
Q.54. असामान्य व्यवहार किन्हीं दो मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन करें।
Ans ⇒ असामान्य व्यवहार के दो मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं —
(क) व्यक्तिगत अपरिपक्वता – असामान्य व्यक्ति का व्यवहार उसकी शिक्षा, आयु एवं सामाजिक स्थिति के अनुसार न होकर कुछ निम्न स्तर का रहता है। उसकी संवेगात्मक अनुभूति तथा अभिव्यक्ति उद्दीपक स्थिति के अनुसार नहीं रहा करती है। उसकी क्रियाएँ क्षणिक आवेगों से ही प्रभावित हो जाती हैं।
(ख) असुरक्षा की भावना – असामान्य व्यक्ति अपने आपको असुरक्षित अनुभव करता है। वह जीवन की सामान्य स्थितियों, कठिनाइयों एवं दायित्वों के पालन में अपने आपको उपयुक्त नहीं समझता है। उसमें आत्म विश्वास की कमी रहा करती है।
Q.55. मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है ? अथवा, मानवतावादी चिकित्सा क्या है ?
Ans ⇒ मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा की धारणा है कि मनुष्य की समस्याएँ अस्तित्व से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत संवृद्धि एवं आत्मसिद्धि पाना चाहता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति को अधिक जटिल, संतुलित और समाकलित होने के लिए प्रेरित करती है। आत्मसिद्धि के लिए संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति आवश्यक है। पर समाज और परिवार संवेगों की उस मुक्त अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि उन्हें डर होता है कि संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति से परिवार और समाज को हानि पहुँच सकती है। यह नियंत्रण सांवेगिक समाकलन की प्रक्रिया को निष्फल करके मनोविकृत व्यवहारात्मक एवं नकारात्मक संवेगों को जन्म देती है। इसलिए इसकी चिकित्सा में चिकित्सक का मुख्य काम रोगी की जागरूकता को बढ़ाना है। चिकित्सक एक अतिनिर्णयात्मक, स्वीकृतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है ताकि रोगी अपने संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति कर सके तथा जटिलता, सतुलन कर सके। चिकित्सा की सफलता के लिए रोगी स्वयं उत्तरदायी होता है। चिकित्सक का काम केवल मार्गदर्शन करते हुए रोगियों के प्रयास को सरल बनाना है।
Q.56. मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन करें।
Ans ⇒ मनोवृत्ति निर्माण के मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं –
(i) परिवार एवं विद्यालय का परिवेश – विशेष रूप से जीवन के आरंभिक वर्षों में अभिवन्ति निर्माण करने में माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में विद्यालय का परिवेश मनोवृत्ति निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाता है।
(ii) संदर्भ समूह – संदर्भ समूह एक व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के स्वीकृत नियमों या मानकों को बताते हैं। अंतः ये समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों के अधिगम को दर्शाते हैं।
(iii) व्यक्तिगत अनुभव – अनेक अभिवृत्तियों का निर्माण प्रत्यय व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है जो लोगों के तथा स्वयं के जीवन के प्रति हमारी मनोवृत्ति में प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करता है।
Q.57. द्वितीयक समूह के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans ⇒ द्वितीयक समूह के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः इसका आकार बहुत बड़ा होता है। लिण्डग्रेन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, “द्वितीयक समूह अधिक अवैयक्तिक होता है तथा सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होता है।”
द्वितीयक समूह के मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –
(i) द्वितीयक समूह में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है।
(ii) इसके सदस्यों में आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है।
(iii) प्राथमिक समूह की तुलना में यह कम टिकाऊ होता है।
(iv) समूह के सदस्यों के बीच एकता का अभाव होता है।
(v) इसके सदस्यों में ‘मैं’ का भाव अधिक होता है।
(vi) इसके सदस्य कभी-कभी आमने-सामने होते हैं।
Q.58. एक प्रभावशाली परामर्शदाता का किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans ⇒ एक परामर्शदाता की दो विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –
(i) प्रामाणिकता – प्रामाणिकता का अर्थ है कि आपके व्यवहार की अभिव्यक्ति आपके मूल्यों, भावनाओं एवं आंतरिक आत्मबिंब के साथ संगत होती है।
(ii) दूसरे के प्रति सकारात्मक आदर – एक उपबोध्य परामर्शदाता संबंध में एक अच्छा संबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। .
Q.59. अनुरूपता क्या है ? स्पष्ट करें।
Ans ⇒ जब व्यक्ति समूह दबाव के कारण अपने व्यवहार तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन उस दबाव द्वारा वाछित दिशा में करता है तो उसे अनुरूपता कहा जाता है। क्रेच, क्रचफील्ड तथा बैलेचीके अनुसार, “अनुरूपता का सार है समूह दबावों के सामने झुक जाना” इस प्रकार अनुरूपता में (i) व्यक्ति समूह दबाव के सामने झुक जाता है, (ii) समूह दबाव में समूह के मानक, मूल्यों द्वारा व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है, (iii) इस व्यवहार की उत्पत्ति मानसिक संघर्ष से होती है।
Q.60. सकारात्मक स्वास्थ्य किसे कहते हैं ? स्पष्ट करें।
Ans ⇒ पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक कुशल की अवस्था ही स्वास्थ्य है न कि केवल रोग अथवा अशक्तता का अभाव। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मितियाँ आती है “स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन में उद्देश्य का बोध, आत्मसम्मान, जीवन के कृत्यों में प्रवीणता, दबाव, अभिघात एवं परिवर्तन के प्रति स्थिति स्थापन।” विशेष रूप से जो कारक दबाव के प्रतिरोधक का कार्य करते हैं तथा सकारात्मक स्वास्थ्य को सुकर बनाते हैं वे हैं आहार, व्यायाम, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक चिंतन तथा सामाजिक अवलंब।
Q.61. आक्रामकता के कारण क्या है ?
Ans ⇒ आक्रामकता के निम्नलिखित कारण हैं –
(i)सहज प्रवृत्ति – आक्रामकता मानव में (जैसा कि यह पशुओं में होता है) सहज (अंतर्जात) होती है। जैविक रूप से यह सहज प्रवृत्ति आत्मरक्षा हेतु हो सकती है।
(ii)शरीर क्रियात्मक तंत्र – शरीर-क्रियात्मक तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामकता जनिक कर सकते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क के कुछ ऐसे भागों को सक्रिय करके जिनकी संवेगात्मक अनुभव में भूमिका होती हैं, शरीर-क्रियात्मक भाव प्रबोधन की एक सामान्य स्थिति या सक्रियण की भावना प्रायः आक्रमण के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। भाव प्रबोधन के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, भीड़ के कारण भी आक्रमण हो सकता है, विशेष रूप से गर्म तथा आर्द्र मौसम में।
(iii) बाल-पोषण – किसी बच्चे का पालन किस तरह से किया जाता है वह प्रायः उसी आक्रामकता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, वे बच्चे जिनके माता-पिता शारीरिक दंड का उपयोग करते हैं, उन बच्चों की अपेक्षा जिनके माता-पिता अन्य अनुशासनिक, तकनीकों का उपयोग करते हैं, अधिक आक्रामक बन जाते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कि माता-पिता ने आक्रामक व्यवहार का एक आदर्श उपस्थित किया है, जिसका बच्चा अनुकरण करता है। यह इसलिए भी हो सकता है कि शारीरिक दंड बच्चे को क्रोधित तथा अप्रसन्न बना दे और फिर बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है वह इस क्रोध को आक्रामक व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त करता है।
(iv) कुंठा – आक्रामण कुंठा की अभिव्यक्ति तथा परिणाम हो सकते हैं, अर्थात् वह संवेगात्मक स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुँचने में बाधित किया जाता है अथवा किसी ऐसी वस्तु जिसे वह पाना चाहता है, उसको प्राप्त करने से उसे रोका जाता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य के बहुत निकट होते हुए भी उसे प्राप्त करने से वंचित रह सकता है। यह पाया गया है कि कुठित स्थितियों में जो व्यक्ति होते हैं, वे आक्रामक व्यवहार उन लोगों की अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करते हैं जो कुठित नहीं होते। कुंठा के प्रभाव की जाँच करने के लिए किए गए एक प्रयोग में बच्चों को कुछ आकर्षक खिलौनों, जिन्हें वे पारदर्शी पर्दे (स्क्रीन) के पीछे से देख सकते थे, को लेने से रोका गया। इसके परिणामस्वरूप ये बच्चे, उन बच्चों की अपेक्षा, जिन्हें खिलौने उपलब्ध थे, खेल में अधिक विध्वंसक या विनाशकारी पाए गए।
Q.62. निर्धनता के कारणों का वर्णन करें।
Ans ⇒ निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –
(i) निर्धन स्वयं अपनी निर्धनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस मत के अनुसार, निर्धन व्यक्तियों में योग्यता तथा अभिप्रेरणा दोनों की कमी होती है जिसके कारण वे प्रयास करके उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों के विषय में यह मत निषेधात्मक है तथा उनकी स्थिति को उत्तम बनाने में तनिक भी सहायता नहीं करता है।
(ii) निर्धनता का कारण कोई व्यक्ति नहीं अपितु एक विश्वास व्यवस्था, जीवन-शैली तथा वे मूल्य हैं जिनके साथ वह पलकर बड़ा हुआ है। यह विश्वास व्यवस्था, जिसे ‘निर्धनता की संस्कृति’ (culture of poverty) कहा जाता है, व्यक्ति को यह मनवा या स्वीकार करवा देती है कि वह तो निर्धन ही रहेगा/रहेगी तथा यह विश्वास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है।
(iii) आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारक मिलकर निर्धनता का कारण बनते हैं। भेदभाव के कारण समाज के कुछ वर्गों को जीविका की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अवसर भी दिए जाते। आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक तथा राजनीतिक शोषण के द्वारा वैषम्यपूर्ण (असंगत) तरह से विकसित किया जाता है जिससे कि निर्धन इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ये सारे कारक सामाजिक असुविधा के संप्रत्यय में समाहित किए जा सकते हैं जिसके कारण निर्धन सामाजिक अन्याय, वचन, भेदभाव तथा अपवर्जन का अनुभव करते हैं।
Q. 63. भीड़ अनुभव के लक्षण क्या हैं ?
Ans ⇒ भीड़ का संदर्भ उस असुस्थता की भावना से है जिसका कारण यह है कि हमारे आस-पास बहुत अधिक व्यक्ति या वस्तएँ होती हैं जिससे हमें भौतिक बंधन की अनुभूति होती है तथा कभी-कभी वैयक्तिक स्वतंत्रता में न्यूनता का अनुभव होता है। एक विशिष्ट क्षेत्र या दिक् में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही भीड़ कहलाती है। जब यह संख्या एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाती है तब इसके कारण वह व्यक्ति जो इस स्थिति में फंस गया है, दबाव का अनभव करता है। इस अर्थ में भीड़ भी एक पर्यायवाची दबावकारक का उदाहरण है।
भीड़ के अनुभव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं –
(i) असुरक्षा की भावना,
(ii) वैयक्तिक स्वतंत्रता में न्यूनता या कमी,
(iii) व्यक्ति का अपने आस-पास के परिवेश के संबंध में निषेधात्मक दृष्टिकोण तथा
(iv) सामाजिक अंतःक्रिया पर नियंत्रण के अभाव की भावना।
Q.64. मानव वातावरण के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें।
Ans ⇒ मनुष्य भी अपनी शारीरिरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अन्य उद्देश्यों से भी प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। निर्मित पर्यावरण के सारे उदाहरण पर्यावरण के। ऊपर मानव प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिये, मानव ने जिसे हम ‘घर’ कहते हैं, उसका निर्माण प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके ही किया जिससे कि उन्हें एक आश्रय मिल सके। मनुष्यों के इस प्रकार के कुछ कार्य पर्यावरण को क्षति भी पहुँचा सकते हैं और अंततः स्वयं उन्हें भी अनेकानेक प्रकार से क्षति पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे-रेफ्रीरजेटर तथा वातानुकूलन यंत्र जो रासायनिक द्रव्य (जैसे-सी.एफ.सी. या क्लोरो-फ्लोरो कार्बन) उत्पादित करते हैं, जो वायु को प्रदूषित करने हैं तथा अंततः ऐसे शारीरिक रोगों के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे कैंसर के कुछ प्रकार। धूम्रपान के द्वारा हमारे आस-पास की वायु प्रदूषित होती है तथा प्लास्टिक एवं धातु से बनी वस्तुओं को जलाने से पर्यावरण पर घोर विपदाकारी प्रदूषण फैलाने वाला प्रभाव होता है। वृक्षों के कटान या निर्वनीकरण के द्वारा कार्बन चक्र एवं जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इससे अंततः उस क्षेत्र विशेष में वर्षा के स्वरूप पर प्रभाव पड़ सकता है और भू-क्षरण तथा मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो सकती है। वे उद्योग जो निस्सारी का बहिर्वाह करते हैं तथा इस असंसाधित गंदे पानी को नदियों में प्रवाहित करते हैं, इस प्रदूषण के भयावह भौतिक (शारीरिक) तथा मनोवैज्ञानिक परिणामों से तनिक चिंतित प्रतीत नहीं होते हैं।
Q.65. विच्छेदी स्मृतिलोप का वर्णन करें।
Ans ⇒ विच्छेदी स्मृतिलोप (Dissociative amnesia) में अत्यधिक किन्तु चयनात्मक स्मृतिभ्रंश होता है जिसका कोई ज्ञात आंगिक कारण (जैसे-सिर में चोट लगना) नहीं होता है। कुछ लोग अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। दूसरे लोग कुछ विशिष्ट घटनाएँ, स्थान या वस्तुएँ याद नहीं कर पाते, जबकि दूसरी घटनाओं के लिए उनकी स्मृति बिल्कुल ठीक होती है। यह विकार अक्सर अत्यधिक दबाव से संबंधित होता है।
Q.66. समाजोपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन करें।
Ans ⇒ समाजोपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं –
(i) समाजोपकारी व्यवहार, मनुष्यों की अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्यों की सहायता करने की एक सहज, नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित है। यह सहज प्रवृत्ति प्रजाति की उत्तरजीविता या अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है।
(ii) समाजोपयोगी व्यवहार अधिगम से प्रभावित होता है। लोग जो ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले-बढ़े होते हैं जो लोगों की सहायता करने का आदर्श स्थापित करते हैं, वे सहायता करने की प्रशंसा करते हैं और उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक समाजोपकारी व्यवहार का प्रदर्शन करते है जो एक ऐसे पारिवारिक परिवेश में पले-बढ़े होते हैं जहाँ इन गुणों का अभाव होता है।
Q.67. अभिवृत्ति और विश्वास में अंतर स्पष्ट करें।
Ans ⇒ सामाजिक प्रभाव के कारण लोग व्यक्ति के बारे में तथा जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो उनके अंदर जो एक व्यवहारात्मक प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती है, अभिवृत्ति कहलाती है।
विश्वास, अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिन पर अभिवृत्ति टिकी है; जैसे-ईश्वर में विश्वास।
Q.68. मनोचिकित्सा के नैतिक सिद्धांत का वर्णन करें।
Ans ⇒ कुछ नैतिक सिद्धांत मानक जिनका व्यवसायी मनोचिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए वे हैं –
(i) सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेनी चाहिए।
(ii) सेवार्थी की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए।
(iii) व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनोचिकित्सा के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए।
(iv) चिकित्सक-सेवार्थी संबंध की अखंडता
(v) मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर।
(vi) व्यावसायिक सक्षमता एवं कौशल आवश्यक है।
Q.69. मनोचिकित्साओं के उद्देश्यों का वर्णन करें।
Ans ⇒ मनोचिकित्साओं के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –
(i) सेवार्थी के सुधार के संकल्प को प्रबलित करना।
(ii) संवेगात्मक दबाव को कम करना।
(iii) सकारात्मक विकास के लिए संभाव्यताओं को प्रकट करना।
(iv) आदतों में संशोधन करना।
(v) चिंतन के प्रतिरूपों में परिवर्तन करना।
(vi) आत्म-जागरुकता को बढ़ाना।
(vii) अंतर्वैयक्तिक संबंधों एवं संप्रेषण में सुधार करना।
(viii) निर्णयन को सुकर बनाना।
(ix) जीवन में अपने विकल्पों के प्रति जागरूक होना।
(x) अपने सामाजिक पर्यावरण से एक सर्जनात्मक एवं आत्म-जागरूक तरीके से संबंधित होना।
Q.70. व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म में अंतर करें।
Ans ⇒ व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में ही संबंध होने का अनुभव करता है।
सामाजिक आत्म में सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन अथवा भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है।
Q.71. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करें।
Ans ⇒ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Verbal intelligence test) – जो परीक्षण भाषा अथवा शब्दों द्वारा किये जाते हैं उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है। इन परीक्षणों में परीक्षक परीक्षार्थी से अनेक प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। अतः इनको वाचिक परीक्षण भी कहा जाता है।
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण (Non verbal intelligence test) – इन परीक्षणों में भाषा के प्रयोग के स्थान पर क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। इनमें प्रयोज्य के सामने कुछ विशेष वस्तुएँ प्रस्तुत की जाती हैं। इन प्रयोज्यों से कुछ इधर-उधर घुमाकर दी गई समस्या के समाधान के आधार पर प्रश्न करके प्रयोज्यों की भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा इन परीक्षणों से बुद्धि स्तर का मापन किया जाता है। ऐसे परीक्षण उन व्यक्तियों के बुद्धि के स्तर को मापने के लिये किये जाते हैं जो भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ हों।
Q.72. सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें।
Ans ⇒ सांवेगिक बुद्धि के सम्प्रत्यय को सैलोबी (Salovey) एवं मेयर (Meyer) ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, “अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों का परिवीक्षण करने, उनमें विभेदन करने की योग्यता तथा प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिन्तन तथा व्यवहारों को निर्देशित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है।” सांवेगिक बुद्धिलब्धि (emotional intelligence quotient) का उपयोग किसी व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि की मात्रा बताने में उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार बुद्धि लब्धि (I.Q.) का उपयोग बुद्धि की मात्रा बताने में किया जाता है।
अत: सांवेगिक बुद्धि के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि इसके उपयोग से विद्यार्थियों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में सहयोगी व्यवहार के स्थायित्व एवं समाज विरोधी गतिविधियों का ह्रास करने में विद्यार्थियों द्वारा उपयोग अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ है क्योंकि इस प्रकार
की गतिविधियाँ बाह्य जगत की चुनौतियों का सामना करने में अत्यधिक सिद्ध होती हैं।
Q.73. लिबिडो क्या है ? अथवा, कामवृत्ति क्या है ?
Ans ⇒ कामवृत्ति (Libido) के स्थित होने के स्थान और उसकी सफलता एवं असफलता के परिणामस्वरूप ही क्रमशः सामान्य और असामान्य व्यवहारों के विकसित होने की संभावना बनती है।
(a) मौखिक अवस्था (Oral stage) – इस अवस्था में कामवृत्ति (Libido) बच्चे के ओंठ तथा दाँत में रहता है। दूध पीने, खाने या दाँत से काटने पर लिबिडो के स्पर्श से बच्चे को कामानन्द प्राप्त होता है।
(b) गुदा अवस्था (Anal stage) – गुदा अवस्था में बच्चे की गुदा में लिबिडो स्थित रहता है। मल-मूत्र करते समय या रोककर रखने से लिबिडो स्पर्श होता है जिससे बच्चे को लैंगिक आनंद प्राप्त होता है।
(c) यौन प्रधान अवस्था (Phallic stage) – बच्चे की ज्ञानेन्द्रियों के ऊपरी भाग में लिबिडो यौन प्रधान अवस्था में होता है जिसके कारण ज्ञानेन्द्रियों को रगड़ने पर बच्चे को काम का सुख मिलता है।
(d) अव्यक्त अवस्था (Latency stages) – इस अवस्था तक आते-जाते लिबिडो अव्यक्त तथा निष्क्रिय बन जाता है। इसी कारण इस अवस्था में बच्चे नैतिकता की ओर अग्रसर होते हैं।
(e) जननेन्द्रिय अवस्था (Genital stage) – जननेन्द्रिय अवस्था में लिबिडो गुप्तांग तथा शिशन के भीतरी हिस्से में चला जाता है और विषम जातीय लैंगिकता (Hetero-sexuality) के द्वारा काम का आनन्द प्राप्त होता है।
Q.74. पहचान संकट क्या है ?
Ans ⇒ जब कभी भी आप अपने विषय में विचार करते हैं तो आप अपने आप से यह प्रश्न करते हैं कि ‘आप कौन हैं’ संभवतः इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर यह होगा कि आप एक परिश्रमी तथा प्रसन्नचित्त लड़का/लड़की हैं। यह उत्तर आपको आपकी पहचान जो ‘व्यक्ति कौन है’ इसकी स्वयं की परिभाषा है, के विषय में जानकारी देता है। इस आत्म-परिभाषा में वैयक्तिक गुण; जैसे-परिश्रमी, प्रसन्नचित्त या वे गुण जो दूसरों के समान होते हैं; उदाहरण के लिए, लड़का या लड़की दोनों ही शामिल होते हैं। जबकि हम दूसरे पक्षों को समाज में अन्य व्यक्तियों से होने वाले अन्त:क्रिया के फलस्वरूप अर्जित कर सकते हैं। कभी हम स्वयं को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो अन्य स्थिति में हम स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। पहचान स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए दोनों ही समान रूप से वैध है। पहचान हमारे आत्म-संप्रत्यय का वह पक्ष है जो हमारी समूह सदस्यता पर आधारित है। पहचान व्यक्ति को स्थापित करती है, अभिप्राय यह है कि एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि व्यक्ति क्या है और उसकी स्थिति क्या है और इस तरह समाज में हम कहाँ हैं, इसको जानने में मदद करती है।
Q.75. व्यक्तित्व के प्रकार उपागम के सार तत्व का वर्णन करें।
Ans ⇒ प्रकार उपागम (Type approach) के अनुसार व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं। अन्तर्मुखी व्यक्तित्व (interovert personality) तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व (extrovert personality) का उल्लेख यंग ने किया। इसी प्रकार क्रेश्मर ने पिकनिक, आसथेनिक तथा ऐथलेटिक तीन प्रकारों का उल्लेख किया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के तीन प्रकारों तथा इन्डोमौरफी, मेसोमौरफी तथा एकटोमौरफी का उल्लेख किया। क्रेश्मर तथा शेल्डन के उपागम में काफी समानता है, जबकि युग के उपागम में अधिक अपवर्तता है।
| S.N | Class 12th Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 1. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 1 |
| 2. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 2 |
| 3. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 3 |
| 4. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 4 |
| 5. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 5 |
| 6. | Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 6 |
| S.N | Class 12th Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) |
| 1. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 1 |
| 2. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 2 |
| 3. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 3 |
| 4. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 4 |
| 5. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 5 |
| 6. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 6 |
| 7. | Psychology ( दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ) PART – 7 |