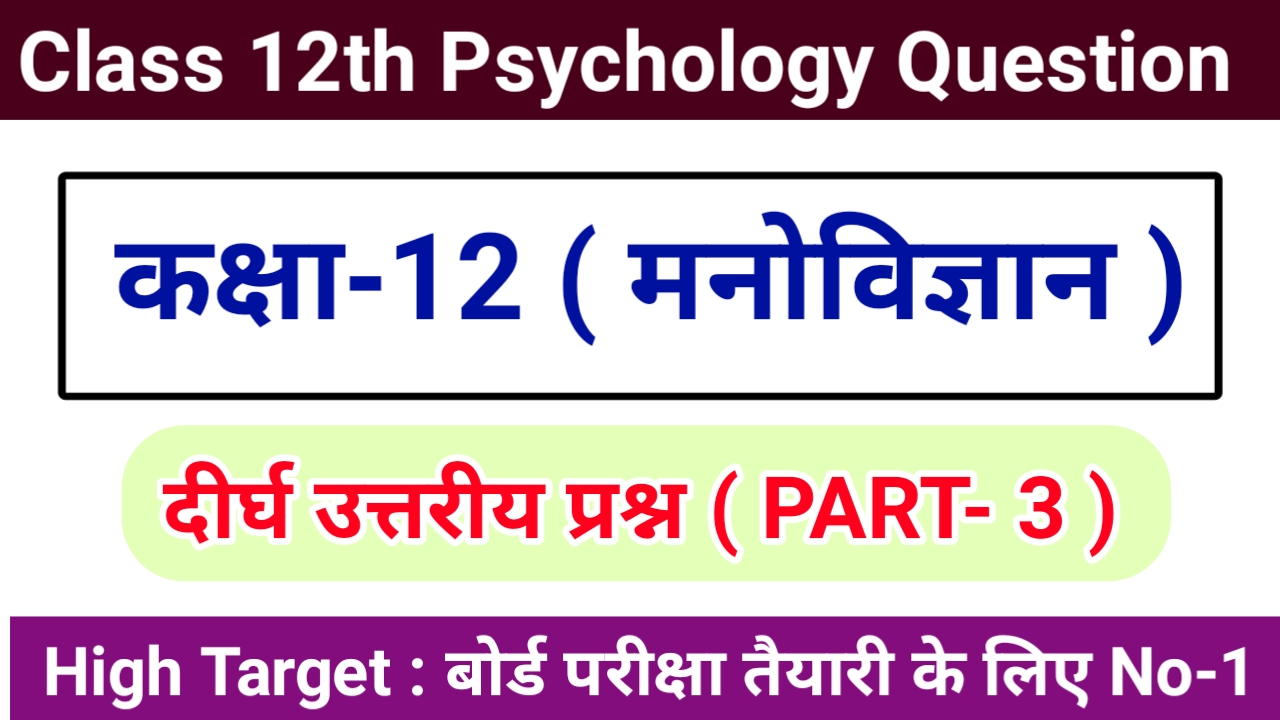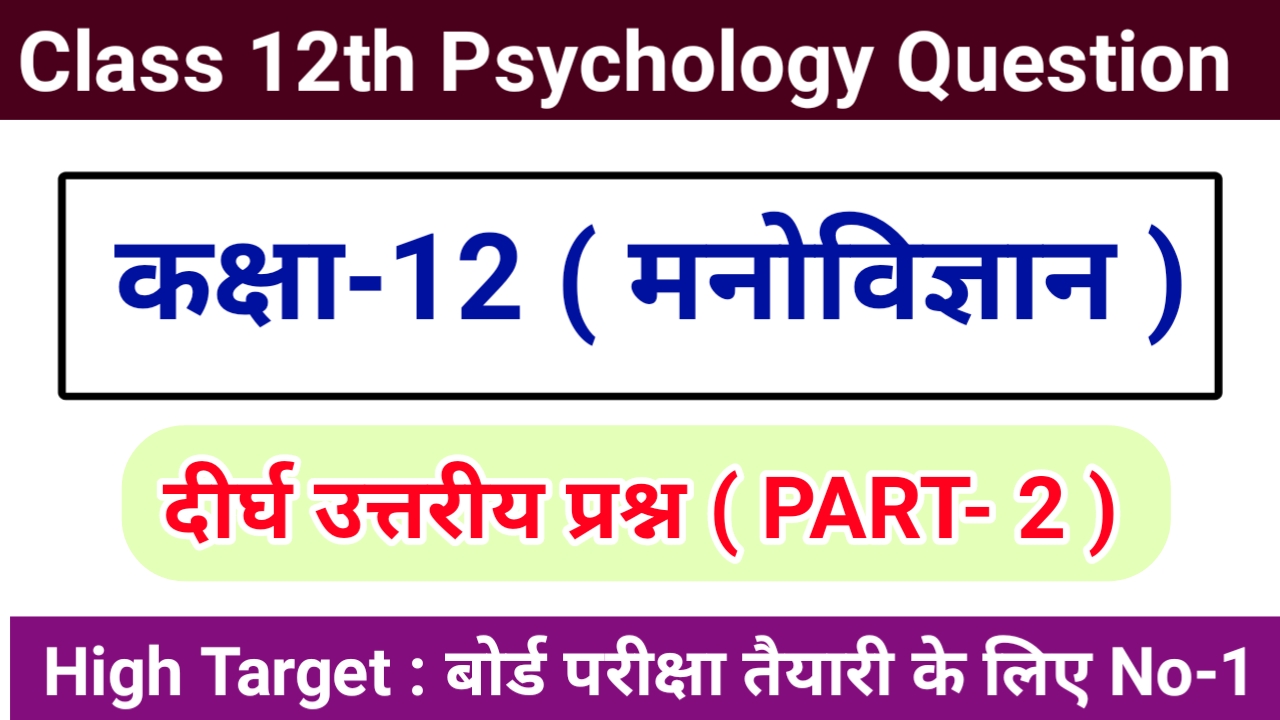Class 12th Psychology ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) PART- 1
Q.1. किस प्रकार मनोवैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण और उसे परिभाषित करते हैं ?
Ans ⇒ मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के स्वरूप को बिल्कुल भिन्न ढंग से समझ जाता है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि के विषय पर शोधकार्य करनेवाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। वेश्लर जिनका बनाया गया बुद्धि परीक्षण बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ने बुद्धि को उसकी प्रकार्यात्मकता के रूप में समझा अर्थात् उन्होंने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने में बुद्धि के मूल्य को महत्व प्रदान किया। वेश्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सोद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों, जैसे-गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उनमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है।
Q.2. किस प्रकार शाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षणों में भेद कर सकते हैं ?
Ans ⇒ शाब्दिक परीक्षणों में परीक्षार्थी को मौखिक अथवा लिखित रूप में शाब्दिक अनुक्रियाएँ करनी होती हैं। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है।
निष्पादन परीक्षण में कोई कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तुओं या अन्य सामग्रियों का प्रहस्तन करना होता है। एकांशों का उत्तर देने के लिए लिखित भाषा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए कोह (Kohs) के ब्लॉक डिजाइन परीक्षण (Block design test) में लकड़ी के कई घनाकार गुटके होते हैं परीक्षार्थी को दिए गए समय के अंतर्गत गुटकों को इस प्रकार बिछाना होता है कि उनसे दिया गया डिजाइन बन जाए। निष्पादन परीक्षणों का एक लाभ यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है।
Q.3. परितोषण के विलंब से क्या तात्पर्य है ? इसे क्यों वयस्कों के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है ? अथवा आत्म-नियमन पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखिए।
Ans ⇒ आत्म-नियमन का तात्पर्य हमारे अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या मॉनीटर करने की योग्यता से है। जिन लोगों में बाह्य पर्यावरण की माँगों के अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है, वे आत्म-परिवीक्षण में उच्च होते हैं।
जीवन की कई स्थितियों में स्थितिपरक दबावों के प्रति प्रतिरोध और स्वयं पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह संभव होता है उस चीज के द्वारा जिसे हम सामान्यतया ‘संकल्प शक्ति’ के रूप में जानते हैं। मनुष्य रूप में हम जिस तरह भी चाहें अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम प्रायः अपनी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि को विलंबित अथवा स्थगित कर देते हैं। आवश्यकताओं के परितोषण की विलंबित अथवा स्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही आत्म-नियंत्रण कहा जाता है। दीर्घावधि लक्ष्यों की संप्राप्ति में आत्म-नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएँ हमें कुछ ऐसे प्रभावी उपाय प्रदान करती हैं जिससे आत्म-नियंत्रण का विकास होता है। (उदाहरणार्थ, व्रत अथवा रोजा में उपवास करना और सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति का भाव रखना)।
आत्म-नियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीकें सुझाई गई हैं। अपने व्यवहार का प्रेक्षण एक तकनीक है जिसके द्वारा आत्म के विभिन्न पक्षों को परिवर्तित, परिमार्जित अथवा सशक्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। आत्म-अनुदेश एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है। हम प्राय: अपने आपको कुछ करने तथा मनोवांछित तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुदेश देते हैं। ऐसे अनुदेश आत्म नियमन में प्रभावी होते हैं। आत्म-प्रबलन एक तीसरी तकनीक है। इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार पुरस्कृत होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हमने अपनी परीक्षा में अच्छा निष्पादन किया है तो हम अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने जा सकते हैं। ये तकनीकें लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और आत्म-नियमन और आत्म-नियंत्रण के संदर्भ में अत्यन्त प्रभावी मानी गई हैं।
Q.4. व्यक्तित्व को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं ? व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन-से हैं ?
Ans ⇒ व्यक्तित्व का तात्पर्य सामान्यतया व्यक्ति के शारीरिक एवं बाह्य रूप से होता है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। लोग सरलता से इस बात का वर्णन कर सकते हैं कि वे किस तरीके के विभिन्न स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कुछ सूचक शब्दों (जैसे-शर्मीला, संवेदनशील, शांत, गंभीर, स्फूर्त आदि) का उपयोग प्रायः व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये शब्द व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों को इंगित करते हैं। इस अर्थ में व्यक्तित्व से तात्पर्य उन अनन्य एवं सापेक्ष रूप से स्थिर गुणों से है जो एक समयावधि में विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की विशिष्टता प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तियों की उन विशेषताओं को भी कहते हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में प्रकट होती हैं।
व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं –
(i) प्रारूप उपागम (ii) विशेषक उपागम (iii) अंतःक्रियात्मक उपागम।
Q.5. व्यक्तित्व का विशेषक उपासक क्या है ? यह कैसे प्रारूप उपागम से भिन्न है ?
Ans ⇒ ये सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन अथवा विशेषीकरण से संबंधित होते हैं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व का निर्माण करनेवाले मूल तत्वों की खोज करते हैं। मनुष्य व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी उनको व्यक्तित्व विशेषकों के लघु समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। विशेषक उपागम हमारे दैनिक जीवन के सामान्य अनुभव के बहुत समान है। उदाहरण के लिए जब हम यह जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक है तो वह व्यक्ति न केवल सहयोग, मित्रता और सहायता करनेवाला होगा बल्कि वह अन्य सामाजिक घटकों से युक्त व्यवहार प्रदर्शित करने में भी प्रवृत्त होगा। इस प्रकार, विशेषक उपागम लोगों की प्राथमिक विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करता है। एक विशेषक अपेक्षाकृत एक स्थिर और स्थायी गुण माना जाता है जिस पर एक व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। इसमें संभव व्यवहारों की एक श्रृंखला अंतर्निहित होती है जिसको स्थिति की माँगों के द्वारा सक्रियता प्राप्त होती है।
विशेषक उपागम प्रारूप उपागम से भिन्न है। व्यक्तिगत के प्रारूप. समानताओं पर आधारित प्रत्याशित व्यवहारों के एक समुच्चय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन काल से ही लोगों को व्यक्तित्व के प्रारूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। हिप्पोक्रेटस ने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड अथवा ह्यूमस पर आधारित है। उन्होंने लोगों को चार प्रारूपों में वर्गीकृत किया है। जैसे-उत्साही, श्लैष्मिक, विवादी और कोपशील। प्रत्येक प्रारूप विशिष्ट व्यवहारपरक विशेषताओं वाला होता है।
Q.6. उन पर्यावरणी कारकों का वर्णन कीजिए जो (अ) हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव तथा (ब) नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
Ans ⇒ विभिन्न पर्यावरणी कारक हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं जबकि ऐसे भी पर्यावरणी कारक हैं जो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, ग्रीष्मकाल की गर्मी, शीतकाल की सर्दी इत्यादि आदि पर्यावरणी दबाव हमारे परिवेश की वैसी दशाएँ होती हैं जो प्रायः अपरिहार्य होती है। इनका हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कुछ पर्यावरणी दबाव प्राकृतिक विपदाएं तथा विपाती घटनाएँ हैं और उनका हमारे ऊपर लंबे अंतराल तक नकारात्मक प्रभाव रहता है। आग, भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, सुनामी आदि इनमें शामिल हैं।
Q.7. अवसाद और उन्माद से संबंधित लक्षणों की पहचान कीजिए।
Ans ⇒ अवसाद – इसमें कई प्रकार के नकारात्मक भावदशा और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। इनके लक्षणों में अधिकांश गतिविधियों में रुचि या आनंद नहीं रह जाता है। साथ ही अन्य लक्षण भी हो सकते हैं; जैसे-शरीर के भार में परिवर्तन, लगातार निद्रा से संबंधित समस्याएँ, थकान, स्पष्ट रूप से चिंतन करने में असमर्थता, क्षोभ, बहुत धीरे-धीरे कार्य करना तथा मृत्यु और आत्महत्या के विचारों का आना, अत्यधिक दोष या निकम्मेपन की भावना का होना।
उन्माद – इससे पीड़ित व्यक्ति उल्लासोन्मादी, अत्यधिक सक्रिय, अत्यधिक बोलनेवाले तथा आसानी से चित्त-अस्थिर हो जाते हैं, उन्माद की घटना या स्थिति स्वतः कभी-कभी ही दिखाई देती है, इनका परिवर्तन अवसर अवसाद के साथ होता रहता है।
Q.8. अतिक्रियाशील बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा, आवेगशील बच्चों की विशेषताओं को लिखिए।
Ans ⇒ जो बच्चे आवेगशील (impulsive) होते हैं वे अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते या काम करने से पहले सोच नहीं पाते। वे प्रतीक्षा करने में कठिनाई महसस करते हैं। या अपनी बारी आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते, अपने तात्कालिक प्रलोभन को रोकने में कठिनाई होती है या परितोषण में विलंब या देरी सहन नहीं कर पाते। छोटी घटनाएँ जैसे चीजों को गिरा देना काफी सामान्य बात है जबकि इससे अधिक गंभीर दुर्घटनाएँ और चोटें भी लग सकती हैं। अतिक्रिया (Hyperactivity) के भी कई रूप होते हैं। ए० डी० एच० डी० वाले बच्चे हमेशा कुछ-न-कुछ करते रहते हैं। इस पाठ के समय स्थिर या शांत बैठे रहना उनके लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा चुलबुलाहट कर सकता है, उपद्रव कर सकता है, कमरे में ऊपर चढ़ सकता है या यों ही कमरे में निरुद्देश्य दौड़ सकता है। माता-पिता और अध्यापक ऐसे बच्चे के बारे में कहते हैं कि उसके पैर में चक्की लगी है, जो हमेशा चलता रहता है तथा लगातार बातें करता रहता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में यह चार गुना अधिक पाया जाता है।
Q.9. समूह हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं ? अथवा, सामाजिक प्रभाव पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
Ans ⇒ समूह एवं व्यक्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव हम लोगों को अपने व्यवहार को एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सामाजिक प्रभाव उन प्रक्रमों को इंगित करता है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार एवं अभिवृत्तियाँ दूसरे लोगों को काल्पनिक या वास्तविक उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। दिन भर में हम अनेक ऐसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें दूसरों ने हमें प्रभावित करने का प्रयास किया हो और हमें उस तरीके से सोचने को विवश किया हो जैसा वे चाहते हैं। माता-पिता, अध्यापक, मित्र, रेडियो तथा टेलीविजन करते हैं। सामाजिक प्रभाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कुछ स्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें दूसरों ने हमें प्रभावित करने का प्रयास किया हो और हमें उस तरीके से सोचने को विवश किया हो जैसे वे चाहते हैं। कुछ स्थितियों में लोगों पर सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक प्रबल होता है जिसके परिणामस्वरूप हमलोग उस प्रकार के कार्य करने की ओर प्रवृत्त होते हैं जो हम दूसरी स्थितियों में नहीं करते। दूसरे अवसरों पर हम दूसरे लोगों के प्रभाव को नकारने में समर्थ होते हैं और यहाँ तक कि हम उन लोगों का अपने विचार या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपना प्रभाव डालते हैं।
Q. 10. मादक द्रव्यों के दुरुपयोग तथा निर्भरता से आप क्या समझते हैं ?
Ans ⇒ मादक द्रव्य दुरुपयोग (Substance abuse) में बारंबार घटित होने वाले प्रतिकूल या हानिकारक परिणाम होते हैं जो मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित होते हैं। जो लोग नियमित रूप से मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनके पारिवारिक और सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं, वे कार्य स्थान पर ठीक से निष्पादन नहीं कर पाते तथा दूसरों के लिए शारीरिक खतरा उत्पन्न करते हैं।
मादक द्रव्य निर्भरता (Substance dependence) में जिस मादक द्रव्य का व्यसन होता है उसके सेवन के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती है, व्यक्ति सहिष्णुता और विनिवर्तन लक्षण प्रदर्शित करता है तथा उसे आवश्यक रूप से उस मादक द्रव्य का सेवन करना पड़ता है। सहिष्णुता का तात्पर्य व्यक्ति के ‘वैसा ही प्रभाव’ पाने के लिए अधिक-से-अधिक उस मादक द्रव्य के सेवन से है। विनिवर्तन का तात्पर्य मनःप्रभावी (Psychoactive) मादक द्रव्य का सेवन बंद या कम कर देता है। मनःप्रभावी मादक द्रव्य वे मादक द्रव्य हैं जिनमें इतनी क्षमता होती है।
Q.11. समूहों में सामाजिक स्वैराचार को कैसे कम किया जा सकता है ? अपने विद्यालय में सामाजिक स्वैराचर की किन्हीं दो घटनाओं पर विचार कीजिए। आपने इसे कैसे दूर किया ?
Ans ⇒ सामाजिक स्वैराचार को निम्न के द्वारा कम किया जा सकता है –
(i) प्रत्येक सदस्य के प्रयासों को पहचानने योग्य बनाना।
(ii) कठोर परिश्रम के लिए दबाव का बढ़ाना (सफल कार्य निष्पादन के लिए समूह सदस्यों को वचनबद्ध करना)
(iii) कार्य के प्रकट महत्व या मूल्य को बढ़ाना।
(iv) लोगों को यह अनुभव कराना कि उनका व्यक्तिगत प्रयास महत्वपूर्ण है।
(v) समूह ,संतक्तता को प्रबल करना जो समूह के सफल परिणाम के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ाता है।
Q.12. लोग यह जानते हुए भी उनका व्यवहार दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, वे क्यों आज्ञापालन करते हैं ? व्याख्या कीजिए।
Ans ⇒ लोग आज्ञापालन निम्नलिखित कारणों से करते हैं –
(i) लोंग इसलिए आज्ञापालन करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि वे स्वयं के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी नहीं है, वे मात्र आप्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत आदेशों का पालन कर रहे हैं।
(ii) सामान्यतया आप्त व्यक्तियों के पास प्रतिष्ठा का प्रतीक (जैसे-वर्दी, पद-नाम) होता जिसका विरोध करने में लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं।
(iii) आप्त व्यक्ति आदेशों को क्रमशः कम से अधिक कठिन स्तर तक बढ़ाते हैं और प्रारंभिक आज्ञापालन अनुसारणकर्ता को प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करता है। एक बार जब कोई किसी छोटे आदेश का पालन कर देता है तो धीरे-धीरे यह आप्त व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और व्यक्ति बड़े आदेशों का पालन करना प्रारंभ कर देता है।
(iv) अनेक बार घटनाएँ शीघ्रता से बदलती रहती हैं, जैसे-दंगे की स्थिति में, कि एक व्यक्ति के पास विचार करने के लिए समय नहीं होता है, उसे मात्र ऊपर से मिलनेवाले आदेशों का पालन करना होता है।
Q.13. परामर्शी साक्षात्कार का विशिष्ट प्रारूप क्या है ?
Ans ⇒ परामर्शी साक्षात्कार के विशिष्ट प्रारूप निम्न प्रकार से होते हैं –
(i) साक्षात्कार का प्रारंभ – इसका उद्देश्य यह होता है कि साक्षात्कार देनेवाला आराम की स्थिति में आ जाए। सामान्यतः साक्षात्कारकर्ता बातचीत की शुरुआत करता है और प्रारंभिक समय में ज्यादा बात करता है।
(ii) साक्षात्कार का मुख्य भाग – यह इस प्रक्रिया का केन्द्र है। इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता सूचना और प्रदत्त प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछने का प्रयास करता है जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है।
(iii) प्रश्नों का अनुक्रम – साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की सूची तैयार करता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों या श्रेणियों से, जो वह जानना चाहता है, प्रश्न होते हैं।
(iv) साक्षात्कार का समापन – साक्षात्कार का समापन करते समय साक्षात्कारकर्ता ने जो संग्रह किया है उसे उसका सारांश बताना चाहिए। साक्षात्कार का अंत आगे के लिए जानेवाले कदम पर चर्चा के साथ होना चाहिए। जब साक्षात्कार समाप्त हो रहा हो तब साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देनेवाले को भी प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए या टिप्पणी करने का मौका देना चाहिए। ।
Q.14. एक सेवार्थी परामर्शदाता संबंधों के नैतिक मापदण्ड क्या है ?
Ans ⇒ एक सेवार्थी परामर्शदाता संबंधों के नैतिक मापदण्ड निम्नलिखित हैं –
(i) भौतिक/व्यावसायिक आचरण-संहिता, मानक तथा दिशा-निर्देशों का ज्ञानः संविधियों, नियमों एवं अधिनियमों की जानकारी के साथ मनोविज्ञान के लिए जरूरी कानूनों की जानकारी भी आवश्यक है।
(ii) विभिन्न नैदानिक स्थितियों में नैतिक एवं विधिक मुद्दों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना।
(iii) नैदानिक स्थितियों में अपनी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार को नैतिक विमाओं को पहचानना और समझना।
(iv) जब भी नैतिक मुद्दों का सामना हो तब उपयुक्त सूचनाओं एवं सलाह को प्राप्त करना।
(v) नैतिक मुद्दों से संबंधित उपयुक्त व्यावसायिक आग्रहिता का अभ्यास करना।
Q. 15. भारतीय संस्कृति में बुद्धि के स्वरूप को लिखें।
Ans ⇒ बौद्धिक प्रतिभाओं और कौशलों का निर्धारण उस सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में होता है जिसमें उसका पालन-पोषण होता है। बुद्धि को अभियोजन की क्षमता माना गया है, अर्थात् जो व्यक्ति जिस समाज में या संस्कृति में पलता है वहाँ उसे अभियोजन करना होता है। चूंकि अलग-अलग संस्कृति के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिमान अलग-अलग होते हैं, अतः वहाँ बुद्धि प्रदर्शन भी अपनी-अपनी संस्कृति एवं समाज के अनुरूप करता है। अत: यह मानना गलत नहीं होगा कि विभिन्न संस्कृतियों में बुद्धि अलग-अलग व्यवहारों द्वारा परिभाषित होती है क्योंकि किसी समाज एवं संस्कृति में किस व्यवहार को लाभप्रद एवं अर्थपूर्ण माना गया है, इसमें अन्तर है। अत: बुद्धि को सांस्कृतिक शैली या सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में देखा जाता है। बुद्धि में कौन-कौन तत्व शामिल होते हैं, इस विषय में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में भिन्नता है।
Q. 16. बहिर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें।
Ans ⇒ बहिर्मुखी व्यक्तित्व युंग द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व प्रकार का एक प्रमुख भाग है। बहिर्मखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक सामाजिक एवं खुशमिजाज प्रकृति के होते हैं। इनमें परोपकारिता का गुण अधिक पाया जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ऐसे लोग आशावादी प्रकृति के होते हैं तथा वे अपना संबंध यथार्थता (realism) से अधिक रखते हैं। ऐसे लोग खाने-पीने की चीजों में अभिरुचि अधिक लेते हैं तथा वे आराम पसंद करते हैं। ऐसे लोग सफल समाजसेवी, नेता तथा उत्तम कलाकार होते हैं।
Q. 17. मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुणों का वर्णन करें।
Ans ⇒ मनोविश्लेषणात्मक विधि के गुण निम्नलिखित हैं –
(i) विधियों एवं माध्यमों से मूल्यांकन करने की योग्यता।
(ii) निर्णय लेने में प्रदत्त संग्रह करते समय एक प्रणालीबद्ध उपागम की उपयोग क्षमता।
(iii) नैदानिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रदत्तों को समाकलित करना।
(iv) निदान के उपयोग एवं निरूपण की योग्यता।
(v) कौशलों के बढ़ाने एवं अमल में लाने के लिए पर्यवेक्षण के प्रभावी उपयोग की क्षमता।
Q. 18. मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक का वर्णन करें।
Ans ⇒ समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक तथा मानवशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि मनोवृत्ति के निर्माण में संस्कृति की अहम भूमिका है। Ruth and Benedict की पुस्तक ‘Pattermof Culture’ तथा Margaret Mead की पुस्तक ‘Sex and Temperament’ में काफी प्रमाण मिलते हैं जो मनोवृत्ति पर संस्कृति के प्रभावों की पुष्टि करते हैं। संस्कृति की भिन्नता के कारण Arapesh जाति के लोग मैत्रीपूर्ण, सहयोगी, दयालु, उदार एवं शांतिप्रिय तथा न्यूगाइना की मुण्डा गुमर जाति के लोग आक्रामक, प्रतियोगी, लड़ाकू, झगड़ालू, निर्दयी होते हैं। उनकी मनोवृत्ति में अन्तर देखा जाता है।
Q. 19. गौण समूह की विशेषताओं को लिखें।
Ans ⇒ गौण या द्वितीयक समूह के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः इसका आकार बहुत बड़ा होता है। लिण्डरग्रेन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, “द्वितीयक समूह का अधिक अवैयक्तिक होता है तथा सदस्यों के बीच औपचारिक तथा संवेदनात्मक संबंध होता है।” इसकी निम्न विशेषताएँ होती हैं-
(i) द्वितीयक समूह में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है।
(ii) इसके सदस्यों में आपस में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है।
(iii) प्राथमिक समूह की तुलना में यह कम टिकाऊ होता है।
(iv) समूह के सदस्यों के बीच एकता का अभाव होता है।
(v) इसके सदस्यों में ‘मैं’ का भाव अधिक होता है।
(vi) इसके सदस्य कभी-कभी आमने-सामने होते हैं।
Q. 20. भू-भागीयता या प्रादेशिकता से आप क्या समझते हैं ?
Ans ⇒ निश्चित भू-भाग या निश्चित प्रदेश को प्रादेशिकता कहते हैं। जैसे-उत्तर प्रदेश के रहने से उत्तर प्रदेश का जिला, उसका भू-भाग एवं निवासी के साथ-साथ भाषा, रहन-सहन सब कुछ का बोध होता है। यह निश्चित भू-भाग है।
Q.21. साक्षात्कार कौशल क्या है ?
Ans ⇒ मनोविज्ञान के क्षेत्र में साक्षात्कार की उपयोगिता में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार को अन्य प्रकार के वार्तालाप की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संज्ञा दी जा सकती है। क्योंकि उसका एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है तथा उसकी संरचना केन्द्रित होती है। साक्षात्कार अनेक प्रकार के होते हैं जैसे- परामर्शी साक्षात्कार, रेडियो साक्षत्कार, कारक परीक्षक साक्षात्कार, उपचार साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार आदि।
Q. 22. क्रेश्मर के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार को लिखें।
Ans ⇒ क्रेश्मर के अनुसार व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार हैं –
(i) प्रारूप उपागम
(ii) विशेषक उपागम तथा
(iii) अंतक्रियात्मक उपागम
Q. 23. असामान्यता का क्या अर्थ है ?
Ans ⇒ असामान्यता सामान्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अतिविकसित या अल्पविकसित या छद्म या विकृत रूप है।” अतः असामान्यता एक अवधारणा (Concept) है, जो असामान्य व्यवहारों एवं अनुभवों की सम्यक् व्याख्या करती है। असामान्यता का प्रकटीकरण व्यक्ति के व्यवहारों द्वारा होता है। असामान्य व्यवहार अनियमित (Irregular) को कहते हैं। यह व्यवहार सामान्य व्यवहार से भिन्न होता है। असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार से विचलित होता है। किस्कर ने असामान्य व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहा है, “मानव के व्यवहार और अनुभूतियाँ जो साधारणतः अनोखी, असाधारण या पृथक् हैं, असामान्य समझी जाती है।”
Q. 24. मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें।
Ans ⇒ जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन से है कि उसके रूप, गंध और स्वाद से मानव के स्वास्थ्य और कृषि उद्योग एवं वाणिज्य को हानि पहुँचे, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार के मानवीय रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें
आँत का रोग, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार तथा पेचिस रोग प्रमुख हैं।
Q. 25. शीलगुण से आप क्या समझते हैं ?
Ans ⇒ व्यक्तित्व का निर्माण अनेक प्रकार के शीलगुणों से होता है। शीलगुण आपस में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, जिनसे व्यक्ति के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन को उचित दिशा एवं गति प्राप्त होती है। इसी कारण इसे सामान्य भाषा में व्यक्ति की विशेषताएँ भी कहा जाता है। व्यक्तित्व की स्थायी विशेषताएँ जिनके कारण उनके व्यवहार में स्थिरता दिखाई पड़ती है, शीलगुण के नाम से जानी जाती है।